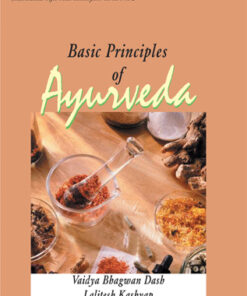Description
जिन धार्मिक घटनाओं ने ब्रजभाषा के सफलतापूर्ण उभार में सहायता की वे मोटे तौर पर एक राजनीतिक प्रक्रिया से मेल खाती थीं। जैसे शहंशाह अकबर के लम्बे शासनकाल के दौरान मुग़ल शासन को मिलने वाली मज़बूती। अकबर की आरम्भिक राजधानी फ़तेहपुर सीकरी और उससे लगा हुआ मुग़ल केन्द्र आगरा पवित्र हिन्दू स्थलों वृन्दावन और मथुरा के क़रीब स्थित था, जिन्हें एक साथ ब्रजमण्डल कहा जाता है, जो उभरते हुए भक्ति आन्दोलन का गढ़ था। जिन राजपूत राजाओं को हाल ही में मुग़ल व्यवस्था में शामिल किया गया था, जिनमें केशवदास के आश्रयदाता ओरछा के बीर सिंह देव बुन्देला, या आमेर के मानसिंह कछवाहा शामिल थे, ये ब्रजमण्डल में मन्दिरों के प्रमुख प्रायोजक थे। वैष्णव समुदायों को जारी किये गये अकबर के फ़रमानों ने भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इस वैष्णव उत्साह और ब्रज में राजपूत और मुग़ल आश्रय के मेल ने ऐसा परिवेश रचा जिसने इस क्षेत्र की भाषा में एक नयी रुचि को विकसित किया। भले ही इसके नाम से यह संकेत मिलता हो कि इसकी उत्पत्ति हिन्दू समुदायों में हुई, ब्रजभाषा आरम्भ से ही बहुमुखी काव्य भाषा थी जिसने कई समुदायों को आकर्षित किया। जैसे वैष्णवों ने भक्तिकविता के लिए ब्रजभाषा का उपयोग किया, वैसे ही अकबर के काल से यह एकाएक और बहुत प्रतिष्ठा के साथ प्रमुख दरबारी भाषा बन गयी। इसी ब्रजभाषा में, और विशेषकर दरबारी परिवेश में रचे गये साहित्य को, इतिहास लेखन की आम सहमति के साथ आधुनिक काल में जाकर रीति साहित्य कहा गया।
—ऐलिसन बुश, इसी पुस्तक से
★★★
वैष्णव सांस्कृतिक सन्दर्भ में उभरी ब्रजभाषा को केशवदास आदि रीति कवियों ने ऐतिहासिक चरित काव्य, दरबारी महाकाव्य, छन्द, अलंकार और रस शास्त्र, कवि-वंश लेखन, राज-वंशावली, राजप्रशस्ति, भव्य और सचित्र पाण्डुलिपियों, हिन्दुस्तानी संगीत, नगर वर्णन व तीर्थाटन, योग साधना, आयुर्वेद व युद्धनीति के सैकड़ों ग्रन्थों की भाषा बनाया। सोलहवीं सदी से उन्नीसवीं सदी तक ब्रजभाषा राजस्थान से लेकर असम और हिमाचल से लेकर दक्कन तक के भूभाग में उच्च अभिरुचि के काव्य और अभिव्यक्ति की भाषा बन गयी थी। शैल्डन पॉलक के शब्दों में कहें तो यह एक ‘कॉस्मोपॉलिटन वर्नाक्यूलर’ या सार्वदेशिक देशभाषा बन चुकी थी। दुर्भाग्य से आधुनिक काल में ब्रजभाषा को हिन्दी की एक ‘बोली’ बता दिया गया और इसका अध्ययन उन हिन्दी विभागों में सीमित रह गया जिनके अपने संकुचित मानदण्ड थे। इसका पुनर्मूल्यांकन किये बिना भारत में इतिहास लेखन की परम्पराओं को समझा नहीं जा सकता और भारत में ‘इतिहास न होने’ के हेगेलियन और जेम्स मिल्सियन पूर्वाग्रहों को तोड़ा नहीं जा सकता। ऐलिसन बुश के अनुसार रीति कविता और ‘कोर्ट कल्चर’ या दरबारी परिवेश एक-दूसरे पर आश्रित थे। बृहत्तर हिन्दुस्तान में फैली यह साहित्यिक संस्कृति बहुभाषी व समावेशी थी। इसलिए रीति कविता को जाने बिना भारत के बहुलतावादी अतीत को समग्रता में नहीं समझा जा सकता।
—दलपत राजपुरोहित, ‘भूमिका’ से
★★★
ऐलिसन बुश ने रीति कविता को पुनःपरिभाषित करते हुए इसे खुद कवियों और आश्रयदाताओं की दृष्टि से देखा कि उनके लिए क्या महत्त्वपूर्ण था? वे किस बात को महत्त्व देते थे और क्यों? इन सवालों ने उन्हें रीतिकाव्य के विशाल आर्काइव को नये सिरे से देखने का अवसर दिया। हिन्दी कवि लगभग चार शताब्दियों तक इसी काव्य संसार की रचना में लगे रहे थे जिससे यह आर्काइव विशाल बनता गया। ऐलिसन बुश ने रीति कवियों के उन शब्दों, विषयों, और छन्दों पर गहराई से काम किया, जिनसे यह काव्य जीवन्त हुआ। अपनी इस पुस्तक में वे कविता और इतिहास के अन्तः सम्बन्धों को दर्शाती हैं।
—फ़्रांचेस्का ऑर्सीनी, अंग्रेज़ी संस्करण की भूमिका से